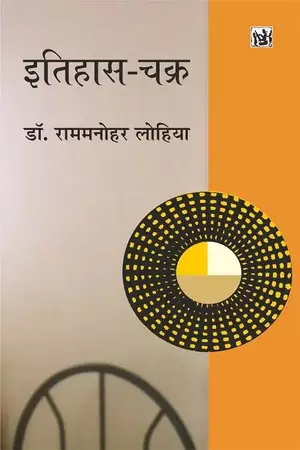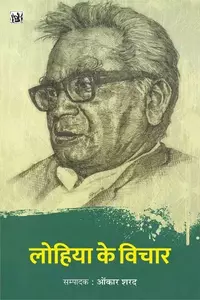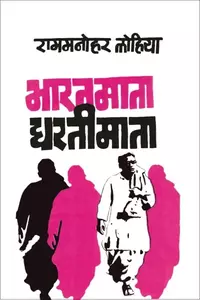|
इतिहास और राजनीति >> इतिहास चक्र इतिहास चक्रराममनोहर लोहिया
|
365 पाठक हैं |
|||||||
"**राममनोहर लोहिया की ऐतिहासिक दृष्टि : सत्ता की राजनीति से परे, समाज और इतिहास की गहराई में**"
Itihas Chakra - A Hindi Book - by Rammanohar Lohiya
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
डॉ. लोहिया के चालीस साल के राजनीतिक जीवन में कभी उन्हें देश में सही माने में नहीं समझा गया। जब देश ने उन्हें समझा और उनके प्रति लोगों में चाह बढ़ी, लोगों ने उनकी ओर आशा की निगाहों से देखना शुरू किया तो अचानक ही वे चले गये। हाँ जाते-जाते अपना महत्त्व लोगों के दिलों में जमा गये।
लोहिया का महत्त्व ! उन्हें गये इतना समय बीत गया, देश की राजनीति में कितना परिवर्तन आ गया। फिर भी आज जैसे नए सिरे सो लोहिया की जरूरत महसूसस की जा रही है। यह तो भावी इतिहास ही सिद्ध करेगा कि देश में आए आज के परिवर्तन में लोहिया की क्या भूमिका रही है। लगता है कि लोहिया ऐसे इतिहास-पुरुष हो गए हैं, जैसे-जैसे दिन बीतेंगे, उनका महत्व बढ़ता जाएगा।
* * *
किसी लेखक ने ठीक ही लिखा है- ‘‘डॉ. राममनोहर लोहिया गंगा की पावन धारा थे, जहाँ कोई भी बेहिचक डुबकी लगाकर मन को और प्राण को ताजा कर सकता है।’’
एक हद तक यह बड़ी वास्तविक कल्पना है। सचमुच लोहिया जी गंगा की धारा ही थे—सदा वेग से बहते रहे, बिना एक क्षण भी रुके, बिना ठहरे।
जब तक गंगा की धारा पहाड़ों में भटकती, टकरती रही, किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मैदानी ढाल पर आकर वह धारा तीव्र गति से बहने लगी तो उसकी तरंगों, उसकी वेगवती धारा, उसके हाहाकार की ओर लोगों ने चकित हो कर देखा, पर लोगों को मालूम न था कि उसका वेग इतना तीव्र था कि समुद्र से मिलने में उसे अधिक समय न लगा। शायद उस वेगवती नदी को खुद भी समुद्र के इतने पास होने का अन्दाजा न था।
* * *
लगता है कि इतिहास-पुरुषों के साथ लोहिया का मन का बहुत गहरा रिश्ता था। ऐसे ही लोहिया के कुछ भावुक क्षण होते थे—राजनीति से दूर, पर इतिहास के गर्भ में जब वे डूबते थे, तो दूसरे ही लोहिया होते थे।
यह इस देश का, इस समाज का और आधुनिक राजनीतिक का दुर्भाग्य है कि महान चिन्तक इस संसार से इतनी जल्दी चला गया। यदि लोहिया कुछ वर्षों और जिन्दा रह जाते तो निश्चय ही सामाजिक चरित्र और समाज संगठन में कुछ नए मोड़ आ जाते।
लोहिया का महत्त्व ! उन्हें गये इतना समय बीत गया, देश की राजनीति में कितना परिवर्तन आ गया। फिर भी आज जैसे नए सिरे सो लोहिया की जरूरत महसूसस की जा रही है। यह तो भावी इतिहास ही सिद्ध करेगा कि देश में आए आज के परिवर्तन में लोहिया की क्या भूमिका रही है। लगता है कि लोहिया ऐसे इतिहास-पुरुष हो गए हैं, जैसे-जैसे दिन बीतेंगे, उनका महत्व बढ़ता जाएगा।
* * *
किसी लेखक ने ठीक ही लिखा है- ‘‘डॉ. राममनोहर लोहिया गंगा की पावन धारा थे, जहाँ कोई भी बेहिचक डुबकी लगाकर मन को और प्राण को ताजा कर सकता है।’’
एक हद तक यह बड़ी वास्तविक कल्पना है। सचमुच लोहिया जी गंगा की धारा ही थे—सदा वेग से बहते रहे, बिना एक क्षण भी रुके, बिना ठहरे।
जब तक गंगा की धारा पहाड़ों में भटकती, टकरती रही, किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मैदानी ढाल पर आकर वह धारा तीव्र गति से बहने लगी तो उसकी तरंगों, उसकी वेगवती धारा, उसके हाहाकार की ओर लोगों ने चकित हो कर देखा, पर लोगों को मालूम न था कि उसका वेग इतना तीव्र था कि समुद्र से मिलने में उसे अधिक समय न लगा। शायद उस वेगवती नदी को खुद भी समुद्र के इतने पास होने का अन्दाजा न था।
* * *
लगता है कि इतिहास-पुरुषों के साथ लोहिया का मन का बहुत गहरा रिश्ता था। ऐसे ही लोहिया के कुछ भावुक क्षण होते थे—राजनीति से दूर, पर इतिहास के गर्भ में जब वे डूबते थे, तो दूसरे ही लोहिया होते थे।
यह इस देश का, इस समाज का और आधुनिक राजनीतिक का दुर्भाग्य है कि महान चिन्तक इस संसार से इतनी जल्दी चला गया। यदि लोहिया कुछ वर्षों और जिन्दा रह जाते तो निश्चय ही सामाजिक चरित्र और समाज संगठन में कुछ नए मोड़ आ जाते।
-ओंकार शरद
भूमिका
यदि अपने अब तक के आर्थिक और राजनीतिक सिद्धान्तों के प्रयत्नों के बौद्धिक नतीजों से सबक लूँ तों ऐतिहासिक सिद्धन्तों के बारे में अपने इस प्रबन्ध को प्रकाशित कराने से मुझे बचना चाहिए थे। लेकिन आशा तो अमर है !
इतिहास, लगता है कि यूनानी दुखान्त नाटकों के अटल तर्क की तरह ही चलता है। पाँच हफ्तों की विदेश-यात्रा के बाद, 1953 के आखिर में, एक हवाई-कम्पनी की एक बस में गोरी चमड़ीवाले मर्दों और औरतों के दल में मैं अकेला अश्वेत श्रोता था, जो भारत के कीड़े-मकोडों और उनके काटने से जीवन भर सताने वाली बिमारियों की बड़े विस्तार से चर्चा कर रहा था। मैं काफी देर तक अपनी जबान पर काबू किए रहा, क्योंकि मैंने धीरज रखना सीख लिया है यद्यपि पूरी तरह नहीं। एक मुखर और चपल महिला को मैंने काले नाग की बात बताई जिसके काटने का कोई इलाज ही नहीं। बस में कुछ लोगों ने समझा कि मैं बहुत कड़ुआ हो रहा हूँ। लेकिन मैं शरीर की किसी कड़ुवाहट के प्रति सजग न था लेकिन वास्तव में मेरे अन्दर इतिहास की कड़ुवी दुराहट की वेदना अवश्य प्राप्त थी। मैंने उन लोगों से कहा कि सचमुच भारत दुनिया का सबसे गरीब और गंदा मुल्क है, लेकिन हो सकता है कि सौ साल या इससे कम समय में, योरप और अमेरिका, भारत से इस संदर्भ में स्थान परिवर्तन कर लें। यह तो इतिहास-चक्र है। यह बिना किसी भावना के चलता है मेरे लोग और मेरा देश दो बार पहले ही इतिहास के शिखर पर खड़े हो चुके हैं और मैं नहीं चाहूँगा कि इसकी तीसरी आवृत्ति हो। क्योंकि, यदि शिखर पर चढ़ने का तीसरी बार अवसर आयेगा तो निश्चय ही हम फिर औंधे-मुँह नीचे गिर कर धूल फाँकेगे। यूनानियों और रोमनों को छोड़कर जो किसी तरह भी वर्तमान गोरी सभ्यता का अंग नहीं है, अमरीका और योरप वाले उतार-चढ़ाव के इस व्यापार में बिल्कुल नए ही है। उनकी अपनी कोई अतीत-कुल-स्मृतियाँ नहीं जो उन्हें इतिहास-चक्र की याद दिलाएँ। यही सबसे दुख की बात है। यदि इस चक्र पर सदा स्वयं टूटने के बजाय, मानव जाति की संभावित योजना से इसे ही तोड़ा जाय तो अब भी दुनिया में बुद्धिमानों की वह हँसी गूँज सकती हैं जो मैंने महात्मा गाँधी से सुनी और अलबर्ट आइन्स्टीन में जिनकी प्रतिध्वनि से मुझे प्रफुल्लता मिली थी।
जिबरान मजदलानी, उनकी माँ, उनका शोफर, तीनों ही अरब और हम एक बार, मोटर बेरुत से मश्क जा रहे थे जहां के खेत व पहाड़ियाँ बाइबिल की कथाओं द्वारा पवित्र हो चुके थे। एक बर्र मोटर में घुस आयी। जिबरान की माँ बहुत परेशान हो उठी और मोटर रुकवाई। तब तक बर्र शान्त होकर मेरे किनारे आकर बैठ गई थी। कड़े कागज के एक टुकड़ा उठाकर उसी से, धीरे से मैं बर्र जैसे नखरे दिखाने लगी। जिबरान की माँ अधिक उत्तेजित हो उठीं और मुझसे बोलीं के मैं बर्र को मार डालूँ। मैंने उनसे कहा कि बेचारी खुद ही थोड़े दिनों में मर जाएगी। उनका ख्याल था कि मरने से पहले यह किसी न किसी को डंक मारेगी अवश्य और उन्होंने मुझसे पूछा कि साँप होता तो मैं क्या करता। तब उन्हें यह बताकर कि जानवर या कीड़े जब तब छेड़ें या सताये न जायें प्रायः हमला नहीं करते, मैंने उनसे पूछा कि अकारण डर या घृणा से हमला करने वाले के साथ वे क्या करेंगी ? उन्हों बताया कि वह उसे भी मारने का प्रयत्न करेंगी। मैंने उनसे कहा कि ऐसी हालत में सारी मानव-जाति को ही हमला करने से रोकने के लिए मारना पड़ेगा। इस समय जिबरान ने बीच में पकड़कर अपनी माँ को भारत और गाँधी के बारे में बताया। तब तक बर्र खिड़की से बाहर उड़ गई। वास्तव में बर्रों को बराबर खिड़की से बाहर निकालते रहना होगा और अगर इसमें कोई कमी नहीं हुई तो उनके डंक और उनको मारनेवाले बढ़ते जायेंगे। लेकिन अधिकांश जातियों को मार कर समाप्त करना असंभव है, वे समाप्त हो सकती हैं यदि उनकी पैदाइश रोक दी जाय। कोई बम, हाइड्रोजन बन भी मानव-जाति को इस तरह समाप्त नहीं कर सकता कि सकी पैदाइश रुक जाय। जीवित –प्राणियों में व्याप्त बुराई को अचानक समाप्त नहीं किया जा सकता, अधिक से अधिक उनकी पैदाइश रोकी जा सकती है। अतः बर्रों को बराबर ही खिड़की के बाहर निकालते रहना होगा और उनकी पैदाइश की जगहों को खोज कर साफ करते रहना होगा। क्या कभी मनुष्य को अपने भाग्य की बुराइयों के पैदाइश-स्थल को खोज कर साफ करने में इतिहास पढ़ने से सहायता मिलेगी ?
इतिहास, लगता है कि यूनानी दुखान्त नाटकों के अटल तर्क की तरह ही चलता है। पाँच हफ्तों की विदेश-यात्रा के बाद, 1953 के आखिर में, एक हवाई-कम्पनी की एक बस में गोरी चमड़ीवाले मर्दों और औरतों के दल में मैं अकेला अश्वेत श्रोता था, जो भारत के कीड़े-मकोडों और उनके काटने से जीवन भर सताने वाली बिमारियों की बड़े विस्तार से चर्चा कर रहा था। मैं काफी देर तक अपनी जबान पर काबू किए रहा, क्योंकि मैंने धीरज रखना सीख लिया है यद्यपि पूरी तरह नहीं। एक मुखर और चपल महिला को मैंने काले नाग की बात बताई जिसके काटने का कोई इलाज ही नहीं। बस में कुछ लोगों ने समझा कि मैं बहुत कड़ुआ हो रहा हूँ। लेकिन मैं शरीर की किसी कड़ुवाहट के प्रति सजग न था लेकिन वास्तव में मेरे अन्दर इतिहास की कड़ुवी दुराहट की वेदना अवश्य प्राप्त थी। मैंने उन लोगों से कहा कि सचमुच भारत दुनिया का सबसे गरीब और गंदा मुल्क है, लेकिन हो सकता है कि सौ साल या इससे कम समय में, योरप और अमेरिका, भारत से इस संदर्भ में स्थान परिवर्तन कर लें। यह तो इतिहास-चक्र है। यह बिना किसी भावना के चलता है मेरे लोग और मेरा देश दो बार पहले ही इतिहास के शिखर पर खड़े हो चुके हैं और मैं नहीं चाहूँगा कि इसकी तीसरी आवृत्ति हो। क्योंकि, यदि शिखर पर चढ़ने का तीसरी बार अवसर आयेगा तो निश्चय ही हम फिर औंधे-मुँह नीचे गिर कर धूल फाँकेगे। यूनानियों और रोमनों को छोड़कर जो किसी तरह भी वर्तमान गोरी सभ्यता का अंग नहीं है, अमरीका और योरप वाले उतार-चढ़ाव के इस व्यापार में बिल्कुल नए ही है। उनकी अपनी कोई अतीत-कुल-स्मृतियाँ नहीं जो उन्हें इतिहास-चक्र की याद दिलाएँ। यही सबसे दुख की बात है। यदि इस चक्र पर सदा स्वयं टूटने के बजाय, मानव जाति की संभावित योजना से इसे ही तोड़ा जाय तो अब भी दुनिया में बुद्धिमानों की वह हँसी गूँज सकती हैं जो मैंने महात्मा गाँधी से सुनी और अलबर्ट आइन्स्टीन में जिनकी प्रतिध्वनि से मुझे प्रफुल्लता मिली थी।
जिबरान मजदलानी, उनकी माँ, उनका शोफर, तीनों ही अरब और हम एक बार, मोटर बेरुत से मश्क जा रहे थे जहां के खेत व पहाड़ियाँ बाइबिल की कथाओं द्वारा पवित्र हो चुके थे। एक बर्र मोटर में घुस आयी। जिबरान की माँ बहुत परेशान हो उठी और मोटर रुकवाई। तब तक बर्र शान्त होकर मेरे किनारे आकर बैठ गई थी। कड़े कागज के एक टुकड़ा उठाकर उसी से, धीरे से मैं बर्र जैसे नखरे दिखाने लगी। जिबरान की माँ अधिक उत्तेजित हो उठीं और मुझसे बोलीं के मैं बर्र को मार डालूँ। मैंने उनसे कहा कि बेचारी खुद ही थोड़े दिनों में मर जाएगी। उनका ख्याल था कि मरने से पहले यह किसी न किसी को डंक मारेगी अवश्य और उन्होंने मुझसे पूछा कि साँप होता तो मैं क्या करता। तब उन्हें यह बताकर कि जानवर या कीड़े जब तब छेड़ें या सताये न जायें प्रायः हमला नहीं करते, मैंने उनसे पूछा कि अकारण डर या घृणा से हमला करने वाले के साथ वे क्या करेंगी ? उन्हों बताया कि वह उसे भी मारने का प्रयत्न करेंगी। मैंने उनसे कहा कि ऐसी हालत में सारी मानव-जाति को ही हमला करने से रोकने के लिए मारना पड़ेगा। इस समय जिबरान ने बीच में पकड़कर अपनी माँ को भारत और गाँधी के बारे में बताया। तब तक बर्र खिड़की से बाहर उड़ गई। वास्तव में बर्रों को बराबर खिड़की से बाहर निकालते रहना होगा और अगर इसमें कोई कमी नहीं हुई तो उनके डंक और उनको मारनेवाले बढ़ते जायेंगे। लेकिन अधिकांश जातियों को मार कर समाप्त करना असंभव है, वे समाप्त हो सकती हैं यदि उनकी पैदाइश रोक दी जाय। कोई बम, हाइड्रोजन बन भी मानव-जाति को इस तरह समाप्त नहीं कर सकता कि सकी पैदाइश रुक जाय। जीवित –प्राणियों में व्याप्त बुराई को अचानक समाप्त नहीं किया जा सकता, अधिक से अधिक उनकी पैदाइश रोकी जा सकती है। अतः बर्रों को बराबर ही खिड़की के बाहर निकालते रहना होगा और उनकी पैदाइश की जगहों को खोज कर साफ करते रहना होगा। क्या कभी मनुष्य को अपने भाग्य की बुराइयों के पैदाइश-स्थल को खोज कर साफ करने में इतिहास पढ़ने से सहायता मिलेगी ?
-राममनोहर लोहिया
उद्देश्य और इतिहास
बीस साल से भी ज्यादा पहले, बर्लिन विश्वविद्यालय के रेस्तरां की एक मेज पर इतिहास के कुछ विद्यार्थी बैठे थे। उनमें से कुछ हेगेलवादी थे, कुछ मार्कसवादी। मैंने उनसे यह प्रश्न किया कि अपनी परिपक्व सभ्यता के बावजूद भी भारत दूसरे देश का गुलाम कैसे हो गया ? उनमें कोई हठी या उद्दण्ड न था जैसा कि इतिहास पढ़ने वालों के लिए होगा उचित ही था और मार्क्सवादी ने अपनी समझ से उत्तर दिया। उसने बताया कि भारत की मंडियाँ गाँव के स्तर से बढ़ कर राष्ट्र के पैमाने तक पहुँच नहीं सकीं, भूमिहीन मजदूर देश में बहुत न बढ़ सके, और बड़े पैमाने पर बेदखलियाँ नहीं हुई काफी मात्रा में धंधे बढ़ाने योग्य व्यापारिक पूँजी भी न थी और भारत को मैक्सिको का भाग्य और अन्य स्थानों की लूट का अवसर न मिला। यह काफी तथ्यपूर्ण तथा विस्तृत उत्तर था और जहाँ तक सचाई का सम्बन्ध है कि हद तक सही उत्तर था। ब्रिटिशों द्वारा भारत पर कब्जा जमाने के पहले हमारी मंडियाँ आमतौर पर गाँव के स्तर की थीं, हमारे भूमिहीन मजदूरों की संख्या भी अधिक न थी और जहाँ तक हमारे उद्योग-धंधों के लिए व्यापारी पूँजी का सवाल है, यह विवादग्रस्त विषय है। फिर भी, मैंने अपने उस इतिहास के मार्क्सवादी सह-विद्यार्थी से पूछा कि यह तमाम तथ्य जो उसने गिनाए ये इंग्लैण्ड या पश्चिम योरप के अन्य देशों में सुलभ थे और भारत में क्यों नहीं थे। इसका उसके पास कोई जवाब न था।
तब हेगेलवादी से इस प्रश्न का उत्तर खोजने को कहा गया, और उसने जो कुछ कहने की कोशिश की वह इतिहास की आत्मा के बारे में, और कहा कि किसी कारण से इतिहास की आत्मा उस समय भारत के पक्ष में न थी कि वह विदेशी-आक्रमण के बचाव कर सकता और लोग भी थके हुए थे। लेकिन वह भी असंतोषजनक उत्तर था। इतिहास की दो प्रमुख विचार-धाराओं से, जो इतिहास की गति के सम्बन्ध में अन्तिम बातें या अन्तिम उत्तर देने का दावा रखती हैं, इस प्रकार के उत्तर अजीब थे। अवश्य ही मार्क्सवादी ने जहाँ तक लक्षण या चिन्हों का प्रश्न है, अच्छे उत्तर की कोशिश की थी, लेकिन इन लक्षणों के कारणों के सम्बन्ध में वह भी उतने ही अँधेरे में था जितना कि इतिहास की दूसरी विचारधारा को मानने वाला होता। यदि इस सवाल पर और अधिक जो जोर दिया जाता, तो मार्क्सवादी और हेगेलवादी दोनों ही अपने उत्तरों में शायद अधिक चतुराई, रुक्षता व कठोरता दिखाते। मराक्सवादी शायद कहता कि मानव-इतिहास ने कुछ खास रास्तों से चलकर ही मार्ग ढूँढ़ा है और यह तथ्य कि किन्हीं खास मौकों पर भारत को अन्य दूसरे देशों जैसा सुयोग या सुअवसर नहीं मिला, वह मानवता के लिए भी बहुत महत्त्व का सिद्ध नहीं हो सका। महत्त्वपूर्ण तथ्य की बात इतनी ही है कि प्रगति के तरीकों में मानवता ने क्रम से सीढ़ियाँ पार की हैं। उस विशेष अवसर पर पश्चिमी योरप, भारत से आगे बढ़ा और मैंने जो पूछा था वह उतने महत्व का प्रश्न न था। इसी तरह, हेगेलवदी संभवतः कहता कि भारत के लोगों की विशेष प्रतिज्ञा तत्त्वज्ञान, अराजकता और विचार के क्षेत्र में ही है। अराजकता, जो कुछ अवसरों परम मानवीय आत्मा और संगठन के बहुत बड़े नतीजो की प्राप्ति कराती है, और वहीं दूसरे अवसरों पर, विशेषकर जब लोग विश्व इतिहास में अपनी भूमिका अदा कर चुके होते हैं, और अपनी सृजनात्मक शक्तियों का व्यय कर चुके होते हैं तो उससे प्रगति अवरुद्ध हो जाती है।
इन उत्तरों ने किसी तरह ही हमें इतिहास की गति के सम्बन्ध में कोई सुराग नहीं दिया। प्रश्न अभी भी बना रहता है, कि ऐसा क्यों है कि कुछ विशेष लक्षण या बातों जो कुछ विशेष अवसरों पर प्रभावशाली सिद्ध होती हैं, वही दूसरे अवसरों पर प्रभावहीन क्यों हो जाती है ? क्योंकि जो लोग इस सम्बन्ध में हमें नियम देने का दावा करते हैं या कुछ रोशनी डालना चाहते हैं कि अलग-अलग समय में मानव का विकास कैसे हुआ, उन्हें यह भी बताने को सामर्थ्यवान होना चाहिए कि लोगों और वर्गों का उत्थान और पतन क्यों होता है ? यदि इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है, तो इतिहास के नियम की बात करना फिजूल है। लक्षणों या चिन्हों की बातें करना कारण बताना नहीं होता।
तब हेगेलवादी से इस प्रश्न का उत्तर खोजने को कहा गया, और उसने जो कुछ कहने की कोशिश की वह इतिहास की आत्मा के बारे में, और कहा कि किसी कारण से इतिहास की आत्मा उस समय भारत के पक्ष में न थी कि वह विदेशी-आक्रमण के बचाव कर सकता और लोग भी थके हुए थे। लेकिन वह भी असंतोषजनक उत्तर था। इतिहास की दो प्रमुख विचार-धाराओं से, जो इतिहास की गति के सम्बन्ध में अन्तिम बातें या अन्तिम उत्तर देने का दावा रखती हैं, इस प्रकार के उत्तर अजीब थे। अवश्य ही मार्क्सवादी ने जहाँ तक लक्षण या चिन्हों का प्रश्न है, अच्छे उत्तर की कोशिश की थी, लेकिन इन लक्षणों के कारणों के सम्बन्ध में वह भी उतने ही अँधेरे में था जितना कि इतिहास की दूसरी विचारधारा को मानने वाला होता। यदि इस सवाल पर और अधिक जो जोर दिया जाता, तो मार्क्सवादी और हेगेलवादी दोनों ही अपने उत्तरों में शायद अधिक चतुराई, रुक्षता व कठोरता दिखाते। मराक्सवादी शायद कहता कि मानव-इतिहास ने कुछ खास रास्तों से चलकर ही मार्ग ढूँढ़ा है और यह तथ्य कि किन्हीं खास मौकों पर भारत को अन्य दूसरे देशों जैसा सुयोग या सुअवसर नहीं मिला, वह मानवता के लिए भी बहुत महत्त्व का सिद्ध नहीं हो सका। महत्त्वपूर्ण तथ्य की बात इतनी ही है कि प्रगति के तरीकों में मानवता ने क्रम से सीढ़ियाँ पार की हैं। उस विशेष अवसर पर पश्चिमी योरप, भारत से आगे बढ़ा और मैंने जो पूछा था वह उतने महत्व का प्रश्न न था। इसी तरह, हेगेलवदी संभवतः कहता कि भारत के लोगों की विशेष प्रतिज्ञा तत्त्वज्ञान, अराजकता और विचार के क्षेत्र में ही है। अराजकता, जो कुछ अवसरों परम मानवीय आत्मा और संगठन के बहुत बड़े नतीजो की प्राप्ति कराती है, और वहीं दूसरे अवसरों पर, विशेषकर जब लोग विश्व इतिहास में अपनी भूमिका अदा कर चुके होते हैं, और अपनी सृजनात्मक शक्तियों का व्यय कर चुके होते हैं तो उससे प्रगति अवरुद्ध हो जाती है।
इन उत्तरों ने किसी तरह ही हमें इतिहास की गति के सम्बन्ध में कोई सुराग नहीं दिया। प्रश्न अभी भी बना रहता है, कि ऐसा क्यों है कि कुछ विशेष लक्षण या बातों जो कुछ विशेष अवसरों पर प्रभावशाली सिद्ध होती हैं, वही दूसरे अवसरों पर प्रभावहीन क्यों हो जाती है ? क्योंकि जो लोग इस सम्बन्ध में हमें नियम देने का दावा करते हैं या कुछ रोशनी डालना चाहते हैं कि अलग-अलग समय में मानव का विकास कैसे हुआ, उन्हें यह भी बताने को सामर्थ्यवान होना चाहिए कि लोगों और वर्गों का उत्थान और पतन क्यों होता है ? यदि इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है, तो इतिहास के नियम की बात करना फिजूल है। लक्षणों या चिन्हों की बातें करना कारण बताना नहीं होता।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book